पटना: पटना में आज जो पचास वर्ष के होंगे और उनकी याददाश्त आँख की ज्योति की तरह कमजोर नहीं हुई होगी तो शायद उन्हें अस्सी के दशक के उत्तरार्ध का कालखंड याद होगा मजहरुल हक़ पथ स्थित तत्कालीन केंद्रीय कारा से पूर्व दाहिने हाथ का अंतिम पाँच मंजिला भवन का घेराव। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को डाक बंगला चौराहा, आकाशवाणी के रास्ते गाँधी मैदान से जोड़ने वाली सड़क अपने अंदर आज भी इतिहास के कई अध्याय संजोये बैठी है। हज़ारों की भीड़ लगी थी उस दिन। सड़क पर ‘डालडा’ बनस्पति के विरुद्ध ‘मुर्दावाद – मुर्दावाद’ के नारे बुलंद हो रहे थे। उस दिन दोपहर उस भवन के बगल से अंदर माड़वाड़ी वासा जाने वाली संकीर्ण सड़क पर लोगों का जमाव भयंकर था। बैंक ऑफ़ इंडिया के बाहर जरूरत से अधिक पटना पुलिस के कर्मियों को सुरक्षा के मद्दे नजर तैनात कर दिया गया था। मजहरुल हक़ पथ को आज भी लोग फ़्रेज़र रोड के नाम से जानते हैं।
वैसे इस सड़क का नामकरण ब्रितानिया हुकूमत के कालखंड में तत्कालीन ब्रिटानिया अभियंता जेम्स फ़्रेज़र के नाम पर हुआ, जिन्होंने शहर का विकास किया था। आज़ादी के बाद इसका आधिकारिक नाम महान धर्मशास्त्री, शिक्षाविद्, राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी, वकील मजहरुल हक़ के नाम अंकित हुआ। वैसे आज भी यह सड़क को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को गाँधी मैदान से जोड़ती है, लोगबाग फ़्रेज़र रोड के नाम से ही जानते हैं। वजह भी है – आज़ादी के बाद क्रांतिकारियों, शहीदों, कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र भारत के लोग जानते कहाँ हैं? क्योंकि 140 करोड़ की आवादी में शायद 12 फीसदी लोग ही हैं जो 78+ वर्ष के हैं और देश को आज़ाद होते देखे हैं। और जो देखे देश को आज़ाद होते वे उस दृश्य को कभी अपने होठों तक आने नहीं दिए, घर, परिवार, समाज के लोगों को नहीं बताये। यह भी दुख की बात है।
राज्य की राजधानी में कई अन्य प्रमुख सड़कें हैं, जिनका नाम स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने रखा था और बाद में स्वतंत्र भारत में उनका नाम बदलकर, ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया। लेकिन, लोग अज्ञानता के कारण, अधिकांश समय उन्हें उनके पुराने नामों से ही पुकारते हैं। क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद आज प्रदेश की सरकार साक्षरता दर के ग्राफ को भले 61.8 फीसदी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2 % और महिलाओं की साक्षरता 51.5 फीसदी (राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% से भी नीचे) दिखाए, पटना का मजहरुल हक़ पथ के साथ-साथ गाँधी मैदान गवाह है कि आज भी शिक्षा का प्रसार कागजों पर अधिक हुआ।
दृष्टान्त देखिये – गार्डिनर रोड। यह सड़क आयकर भवन गोलंबर को आर-ब्लॉक गोलंबर को जोड़ती है। गार्डिनर एक ब्रिटिश अधिकारी थे। आज़ादी के बाद इसका नाम बीर चंद पटेल पथ के नाम पर अंकित कर दिया। पटेल साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। लेकिन प्रदेश की राजनीति उन दिनों भी व्यक्तिगत होती थी, आज तो जाति, धर्म, व्यवसाय और बहुत तरह की बातें जुड़ गयी है उसमें। मुख्यमंत्री बनने की सभी काबिलियत रखते थे बीर चंद पटेल जी । लेकिन मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया राजनीति के कारण। चाहिए तो यह कि उनके नाम से सामाजिक शोध संस्थान संग्रहालय बनता। उनकी जीवनी को प्रदेश की शिक्षा पद्धति में, पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाता ताकि आज की ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी वीर चंद पटेल को जान पाती।
डाकबंगला चौराहे से सचिवालय के रास्ते चिड़िया घर की ओर जाने वाली सड़क जहाँ आज न तो ऐतिहासिक डाक बंगला रहा, पहले बेली रोड के नाम से जाना जाता था। इस सड़क का नामकरण सर स्टोर्ट कॉल्विन बैले पर पड़ा था। ब्रिटानिया हुकूमत के कालखंड में वे बिहार और ओड़िसा के पहले लियूटेनैंट गवर्नर थे। वर्षों पहले बेली रोड को नया नाम मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर – नेहरू पथ। लेकिन आज भी आम बोलचाल में लोग इस सड़क को बेली रोड ही कहते हैं।
इसी तरह, गाँधी मैदान को पटना जंक्शन को एक अलग रास्ते से जोड़ने वाली सड़क एग्जिविशन रोड का नामकरण सप्ताह में लगने वाले बाजार के नाम पर पड़ा था। कालखंड आज़ादी के पूर्व का था। समयांतराल इसका नाम ब्रज किशोर पथ हो गया। ब्रज किशोर सिन्हा संविधान सभा के सदस्य थे, साथ ही, राज्य सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किये थे। इसी तरह, बैंक रोड बी.पी. कोइराला मार्ग बन गया और टेलर रोड पीर अली खान मार्ग हो गया और ऐसे दो दर्जन से अधिक सड़क, गली हैं तो राजनेताओं के नाम से गोदना गोदए हुए हैं । खैर।
चलिए वापस मजहरुक हक़ पथ आते हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित थे उस दिन । मसला था डालडा बनस्पति में चर्वी की मिलावट। उन दिनों पटना ही नहीं, बिहार के लोग, यहाँ तक की ग़रीब-गुरबा भी, घी के स्थान पर रोटी के ऊपर, छौंका लगाने में, पूरी जलेबी छानने में डालडा का प्रयोग करते थे। धार्मिक पर्व छठ में भी बिहार का ऐतिहासिक ठेकुआ बनाने में डालडा वनस्पति का इस्तेमाल होता था। पीला रंग का डब्बा, उसके ऊपर खजूर का पेड़ और हिंदी अंग्रेजी में डालडा लिखा प्रदेश के बाजारों पर कब्जा किए बैठा था। पीरबहोर थाना से सटी महेंद्रू घाट की ओर जाने वाली सड़क पर लगने वाला सोमवारी मेला में खानपान बनाने वाले गौरव के साथ कहते थे ‘डालडा’ में बना है। लेकिन उस दिन जब कलकत्ता की ख़बर से स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुई कि डालडा में चर्बी का प्रयोग किया जाता है – लोगों की धार्मिक भावनाएं मजहरुल हक़ पथ पर उतर गई थी। रात में खाये भोजन सड़क पर निकल रही थी उल्टी के रूप में।
उस दिन के दृश्य को देखकर बैरकपुर सैनिक छावनी और मंगल पाण्डे याद आ गए थे। कलकत्ता से करीब 16 मील दूर बैरकपुर की सैनिक छावनी में अचानक विद्रोह की चिंगारी ज्वाला बन गई। आज हम सभी स्वाधीनता संग्राम के लिए ‘प्रथम युद्ध’ की शुरुआत भी कहते हैं। जाने-माने इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी की एक किताब है, ‘डेटलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज’ में उन्होंने लिखा कि 29 मार्च की दोपहर में रेजिमेंट का कोट और धोती पहने मंगल पांडे नंगे पैर एक भरी हुई बंदूक लेकर छावनी में पहुंचे और सैनिकों से चिल्लाकर कहा कि फिरंगी यहां पर है। ये कारतूस काटने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जायेगा। धर्म के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। अंग्रेजों की सेना में इनफील्ड पी- 53 रायफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस, जिसे अपने दांत से खींचना पड़ता था और जो चर्बी से बना था। उस कालखंड में डालडा वनस्पति पर भी आरोप लगाया गया कि डालडा में पशु वसा है और यह खाने के लिए अनुपयुक्त है।
बहरहाल, इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने नाम में ‘L’ अक्षर डालने पर जोर नहीं दिया होता, तो शायद भारत के उस कालखंड का सबसे पसंदीदा वनस्पति घी को ‘दादा’ कहा जाता। ‘दादा’ दरअसल ‘डच’ कंपनी का नाम था जिसने 1930 के दशक में गाय के दूध से बने देसी घी या मक्खन के सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी का आयात भारत में किया था। ‘घी’ एक महंगा उत्पाद था और भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था – सप्ताहांत पर या कोई स्वादिष्ट व्यंजन या मिठाई बनाते समय।
दूसरी ओर, वनस्पति घी एक प्रकार का वनस्पति छोटा करने वाला पदार्थ था जो हाइड्रोजनीकृत या अत्यधिक संतृप्त वनस्पति तेल से बना होता था और देसी घी की नकल करने के लिए बनाया जाता था। लीवर ब्रदर्स, जो अब यूनिलीवर (भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर) है, जानता था कि देसी घी के विकल्प के लिए एक बाजार है, क्योंकि कई भारतीय मुश्किल से घी खरीद पाते थे। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के निर्माता ने 20वीं सदी की शुरुआत में ही यूरोप में खाद्य उत्पादन में प्रवेश कर लिया था और भारत में वनस्पति घी का उत्पादन करना चाह रहे थे। इस उद्देश्य के लिए इसने 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नामक एक कंपनी भी शामिल की थी।
घरेलू वनस्पति घी बाजार में पैठ बनाने के अवसर को भांपते हुए, लीवर ने भारत में ‘दादा’ बनाने के अधिकार खरीद लिए। बिक्री की एक पूर्व शर्त थी: ‘दादा’ नाम बरकरार रखना होगा। बेशक, लीवर ने इसके विपरीत सोचा। उत्पाद पर कहीं न कहीं इसके स्वामित्व की मुहर तो होनी ही थी। इसलिए चतुर उपभोक्ता वस्तु विपणक एक समाधान लेकर आया: लीवर के लिए एल अक्षर को ठीक बीच में रखा गया। इस प्रकार, डालडा का जन्म हुआ, जिसे 1937 में पेश किया गया। लेकिन, लीवर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भारतीय जनता इस बात से कतई सहमत नहीं थी कि घी का कोई विकल्प हो सकता है। घी आमतौर पर खाना पकाने के माध्यम के रूप में या यहां तक कि भोजन पर छिड़कने पर अपना स्वाद और सुगंध देता है।
कहते हैं कि शुरुआती वर्षों में ‘डालडा’ के लिए चुनौती यह थी कि लोगों को यह बताया जाए कि इसका स्वाद देसी घी जैसा ही है, इसमें तलने के गुण भी देसी घी की तरह हैं, लेकिन घी के विपरीत, यह जेब या तालू पर भारी नहीं लगेगा।” यहीं से लीवर की विज्ञापन एजेंसी लिंटास की शुरुआत हुई। लिंटास में डालडा का खाता संभालने वाले हार्वे डंकन ने 1939 में भारत का पहला मल्टी-मीडिया विज्ञापन अभियान बनाया। इसमें थिएटरों में दिखाने के लिए एक छोटी फिल्म, सड़कों पर घूमने के लिए एक गोल टिन के आकार की वैन, पढ़े-लिखे लोगों के लिए प्रिंट विज्ञापन, सैंपलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल और विज्ञापन अभियान के तहत वितरण के लिए विस्तृत पर्चे थे।
‘डालडा’ न केवल अपने व्यापक प्रचार के लिए बल्कि पीले रंग पर हरे ताड़ के पेड़ के विशिष्ट लोगो वाले टिन के कारण भी अलग पहचान बनाने लगा। लीवर ने इन विशिष्ट डिब्बों को अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में पहुँचाया। अलग-अलग उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग आकार के पैक बनाए गए: होटल और रेस्तराँ जैसे संस्थागत उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा चौकोर डिब्बा और घर में इस्तेमाल के लिए छोटे गोल डिब्बे। लीवर ने डालडा को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसे घी के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश किया।
विज्ञापन इतिहासकारों का कहना है कि अपने अस्तित्व के पहले 25-30 वर्षों तक, ‘डालडा’ को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल निर्माताओं से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। 1980 के दशक तक ‘डालडा’ का बाजार पर एकाधिकार था। डालडा ने शुरुआती विवादों को झेला, जैसे कि 1950 के दशक में, जिसमें डालडा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि यह एक “झूठ” था – एक ऐसा उत्पाद जो देसी घी की नकल करता था, लेकिन असली नहीं था। दूसरे शब्दों में, आलोचकों ने तर्क दिया कि डालडा देसी घी का एक मिलावटी रूप है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश भर में जनमत सर्वेक्षण कराने का आह्वान किया, जो अनिर्णायक साबित हुआ। घी में मिलावट रोकने के उपाय सुझाने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बेशक, सालों बाद डालडा को एक और विवाद का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि इसमें पशु वसा है। तब तक, डालडा को “साफ़ तेल” या परिष्कृत वनस्पति तेलों जैसे कि मूंगफली (पोस्टमैन), सरसों, कुसुम (सफोला), सूरजमुखी (सनड्रॉप) और ताड़ के तेल (पामोलीन) से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी।
इन्हें वनस्पति घी के मुकाबले ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक विकल्प माना जाता था। ‘डालडा’ भारतीय रसोई पर अपनी पकड़ खो रहा था और 2003 तक एचयूएल ने इसे अमेरिकी कृषि और खाद्य दिग्गज बंगे को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से कम में बेच दिया था। उस कालखंड में ‘डालडा’ का अधिग्रहण खाद्य तेल बाजार में एक बड़ी छलांग थी। वनस्पति घी की विरासत के कारण कुछ हद तक यह गलत शुरुआत थी। 2007 में डालडा के नाम से खाद्य तेल की रेंज लॉन्च की गई। इसे ‘हसबैंड चॉइस’ टैगलाइन के तहत लॉन्च किया था। 2013 में, ‘डब्बा खाली, पेट भरा’ टैगलाइन के तहत रेंज को फिर से लॉन्च किया और ब्रांड की इस नई स्थिति को बढ़ावा देने के लिए लाइन के ऊपर के अभियानों के अलावा लाइन के नीचे की गतिविधियों को भी व्यापक रूप से चलाया।”
लेकिन कल जब पटना में पिछले 22 वर्षों से ‘स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मूवमेंट’ और ‘ऑक्सीजन गौशाला’ चलाने वाले विनोद सिंह से बात किये तो डालडा या भारतीय विपणन बाजार में उपलब्ध किसी भी वनस्पति अथवा अन्य तरल पदार्थों के बारे में चर्चा नहीं कर, छींटा अस्सी नहीं कर उनका सिर्फ यही कहना था कि ‘हमें देशी’ होना होगा, सोच में भी, उत्पादन में भी और सुरक्षा में भी। पिछले 22 वर्षों से विनोद सिंह-मनोज सिंह और उनका परिवार पटना में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मूवमेंट और ऑक्सीजन गौशाला चला रहे हैं। अपने प्रयास को उन्होंने कभी पेटेंट नहीं कराया। इसका वजह यह है कि सिंह ब्रदर्स कहते हैं कि चूँकि उनका प्रयास सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, पेटेंट का अर्थ है उनपर एकाधिकार। लेकिन उनका मानना है कि यह प्रयास बिहार ही नहीं, भारत के घर-घर तक पहुंचे एक जागरूकता के तहत। उनकी पूरी कोशिश है कि लोग अधिकाधिक स्वस्थ रहें, निरोग रहे। अगर भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश का विकास स्वतः हो जायेगा।
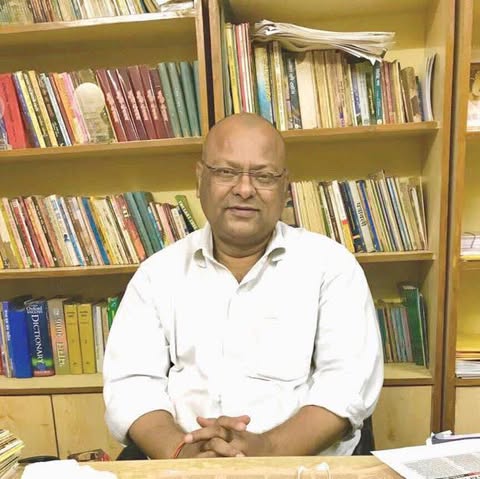
विनोद सिंह कहते हैं कोल्हू द्वारा तैयार तेल सबसे बेहतर है, देसी है, आँखों के सामने निकला जाता है। आप आइये, देखिये, आश्वस्त होइए और अपनी जरूरत के हिसाब से आदेश दीजिये। आपका आदेश न केवल प्रदेश में पशुओं को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि पर्याप्त भोजन के अभाव में घटती प्रजनन क्षमता के कारण देशी नस्ल की गायों की संख्या भी उत्तरोत्तर काम हो रही है।”
ज्ञातव्य हो कि भारत में दस प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में, मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, असम, पंजाब के साथ बिहार भी है। बिहार में सरसों (रबी) का फसल बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा और गया में अधिक होता है जबकि तीसी या अलसी (रबी) के लिए औरंगाबाद, किशनगंज, पश्चिम चंपारण और भभुआ प्रसिद्ध है। तिल (खरीफ / रबी) के मामले में सुपौल, समस्तीपुर, किशनगंज और मधुबनी, सूरजमुखी (रबी) के मामले में मधेपुरा, पूर्णिया, कुसुम (खरीफ / रबी) दरभंगा, मुजफ्फरपुर और खगड़िया और मूंगफली (रबी) के लिए नवादा, पश्चिम चंपारण, गया और नालंदा प्रसिद्ध है। वैसे लोगों का खाना है कि विगत कई वर्षों से लगातार पारंपरिक खेती से मुनाफा अधिक नहीं हो पाने के कारण लोग तिलहन में सरसों की खेती करना शुरू किये हैं। सरसों का मूल्य भी किसानों को अधिक मिलता है।
बिहार के कैमूर को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर किसान धान की खेती होती है। लेकिन यहां भी खेती की क्रिया में लोग परिवर्तन कर रहे हैं – अब किसान अवधान के अलावा गेहूं दलहन और तिलहन की भी खेती करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन गौशाला, जो अपने आप में एक विशेष स्थान और दृष्टान्त रखता है, जैसा कोने-कोने में लघु और कुटीर उद्योगों जैसा विकास होता है तो सरसों का उत्पादन लाभकारी होगा।
वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार कहते हैं कि देशभर में 19.25 करोड़ गाय हैं। देश की कुल गायों की संख्या का 7.95% बिहार में है। यानी बिहार में गायों की संख्या 1.54 करोड़ है। लेकिन, इनमें बिहार की मूल नस्ल की गाय न के बराबर है। हाइब्रिड नस्ल और दूसरे राज्यों से लायी गयी गाय ही बिहार में हैं। गायों की संख्या के लिहाज से देशभर में बिहार चौथे स्थान पर है। लेकिन, राज्यभर में चिह्नित रूप से सिर्फ दो मूल नस्ल की गाय ही शेष रह गयी है। पूर्णिया और बचौर ये दो नस्ल की गाय ही अब बिहार की मूल नस्ल रह गयी है। वर्तमान में दूसरे राज्यों से लायी गयी और हाइब्रिड नस्ल की गायों का ही दूध बिहार के लोग पी रहे हैं।
पूर्णिया नस्ल की गाय पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल में ही कहीं-कहीं मिलेगी। बचौर नस्ल की गाय दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी के क्षेत्रों में ही पायी जाती है। इन दोनों नस्लों की गायों की संख्या लगभग एक से डेढ़ हजार के आसपास होगी। इनका भी संरक्षण नहीं हुआ तो ये नस्लें भी विलुप्त हो जायेंगी। गाय की गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश और बिहार में पायी जाती थी, लेकिन अब बिहार में यह गाय नहीं मिलती है। यह मध्यम आकार की होती है। यह प्रति ब्यांत में औसतन 900-1200 लीटर दूध देती है। इसके दूध में 4.1-5.2 प्रतिशत वसा की मात्रा होती है। वैसे बिहार में गुजरात, पंजाब और राजस्थान की गायों की भरमार है। यहां पंजाब की साहीवाल, राजस्थान की थारपारकर और गुजरात की गिर नस्ल की गाय की भरमार है। राज्य में इस साल इन्हीं नस्लों की गायों की भी सरकारी अनुदान के तहत खरीदारी कर बिहार लाया जा रहा है। बिहार में 7.3% की दर से दूध का उत्पादन हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.29% ही है।
पत्रकार गुलशन सिंह कहते हैं कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देसी गो-पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। देसी गो-पालन प्रोत्साहन योजना से न सिर्फ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि देसी गायों की संख्या में वृद्धि के साथ दूध का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अनुदान का भी प्रावधान किया है। गौ पालन योजना के के माध्यम से सरकार देसी गायों की संख्या में वृद्धि करना चाहती है, इसके लिए सरकार गाय खरीदने पर 50 से 75% तक किसानों को सब्सिडी देगी। इससे राज्य में डेयरी फार्म की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी होगी, इसी के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को एक नया रोजगार भी हासिल होगा। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार राज्य के सभी किसान एवं बेरोजगार युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके माध्यम से दोनों लाभान्वित हो सकेंगे। सरकार यह स्वीकार रही है कि दरअसल समाज में देशी गायों की संख्या में धीरे-धीरे बहुसंख्यक रूप से कम होती जा रही है, जिसके कारण पौष्टिक दूध की भी कमी देखने को मिल रही है। गौ पालन योजना का मुख्य उद्देश्य देसी गायों की संख्या में वृद्धि करना है।
बहरहाल, विनोद सिंह कहते हैं “हम स्वयं या अपने बच्चों को दूध के साथ अन्य कोई वस्तु पीने के लिए क्यों दें ? दूध से अधिक पौष्टिक इस पृथ्वी पर कुछ और है क्या? अन्य पदार्थों को मिलाने से बेहतर है कि दूघ पीने की मात्रा बढ़ाएं। इससे दुघ की मांग भी बढ़ेगी, गौशालाओं की सख्या भी बढ़ेगी, गायों की रक्षा भी होगी और साथ ही, दूध अधिक बिकने से गायों को भर पेट भोजन भी मिलेगा, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगी और अंततः विलुप्त होती गायों को हम रोक पाएंगे। क्योंकि दूध में जो भी हम मिलकर खुद पिटे हैं अथवा बच्चों को देते हैं वह सांप के जहर से भी अधिक खतरनाक है। (समाप्त)




















