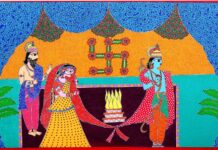बना रहे बनारस का 62 साल हो गया। यानि महादेव भी अब “यादवों वाली कहावत” में आ गए – साठा तब पाठा । बनारस {REVISITING BANARAS} पर कार्य करते समय एक नहीं, करोड़ों ज्ञान-अर्जन हुआ। भगवान् और भक्त में यहीं अन्तर भी समझ पाए। भगवान् को गंगा नहाकर राजनीति में कैसे घसींटा जाता है, यहीं साक्षात दर्शन हुआ। अर्जित ज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ा।
जिस प्रकार हिन्दू धर्म कितना प्राचीन है पता नहीं चलता ठीक उसी प्रकार काशी कितनी प्राचीन है, पता नहीं लग सका। यद्यपि बनारस की खुदाई से प्राप्त अनेक मोहरें, ईंट, पत्थर, हुक्का, चिलम और सुराही के टुकड़ों का पोस्टमार्टम हो चुका है फिर भी सही बात अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है। जन-साधारण में अवश्य काशी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व काशी को शंकर भगवान अपने त्रिशूल पर लादे घूमते-फिरते थे। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गयी तब इसे त्रिशूल से उतारकर पृथ्वी के मध्य में रख दिया गया।
“ठग” के रूप में कलयुग का महान “दार्शनिक ठग” को देखा। क्या अस्सी, क्या तुलसी, क्या राम, क्या राज – बनारस के सभी 84 घाटों पर “नामकरण को लेकर भी” राजनीति देखा। क्या-क्या देखा, लिख नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस स्थान से गंगा उल्टी वापस होती है, उस स्थान पर गंगा की जितनी गहराई है, उतनी ही ह्रदय की गहराई में जो ज्ञानोदय हुआ, वह काशी के बाबू विश्वनाथ मुखर्जी साहेब द्वारा शब्द-बद्ध ‘बना रहे बनारस’ को पढ़कर, समझकर हुआ। इसलिए भगवान् शिव के माथे पर हाथ रखकर सर्वप्रथम उनके प्रति ह्रदय के अन्तः कोने से आभार व्यक्त करते हैं।
पता नहीं, कब किस दिलजले ने इस कहावत “राँड़, साँड, सीढ़ी, संन्यासी – इनसे बचे तो सेवे काशी” को जन्म दिया कि काशी की यह कहावत अपवाद के रूप में प्रचलित हो गयी। इस कहावत ने काशी की सारी महिमा पर पानी फेर दिया है। मुमकिन है कि उस दिलजले का इन चारों से कभी वास्ता पड़ा हो और काफी कटु अनुभव हुआ हो।
खैर, चाहे जो हो, पर यह सत्य है कि काशी आनेवालों का इन चारों से परिचय हो ही जाता है। फिर भी आश्चर्य का विषय यह है कि काशी में आनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो एक बार यहाँ आ बसता है, मरने के पहले टलने का नाम नहीं लेता, जबकि पैदा होनेवालों से कहीं अधिक श्मशान में मुर्दे जलाये जाते हैं। यह भी एक रहस्य है।
इन चारों में सीढ़ी के अलावा बाकी सभी सजीव प्राणी हैं। बेचारी सीढ़ी को इस कहावत में क्यों घसीटा गया है, समझ में नहीं आता। यह सत्य है कि बनारस की सीढ़ियाँ (चाहे वे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर अथवा घर या घाट – किसी की क्यों न हों) कम खतरनाक नहीं हैं, लेकिन यहाँ की सीढ़ियों में दर्शन और अध्यात्म की भावना छिपी हुई है। ये आपको जीने का सलीका और जिंदगी से मुहब्बत करने का पैगाम सुनाती हैं।
अब सवाल है कि वह कैसे? आँख मूँदकर काम करने का क्या नतीजा होता है, अगर आपने कभी ऐसी गलती की है, तो आप वह स्वयं समझ सकते हैं। सीढ़ियाँ आपको यह बताती रहती हैं कि आप नीचे की जमीन देखकर चलिए, दार्शनिकों की तरह आसमान मत देखिए, वरना एक अरसे तक आसमान मैं दिखा दूँगी अथवा कजा आयी है – जानकर सीधे शिवलोक भिजवा दूँगी।
काशी की सीढ़ियाँ चाहे कहीं की क्यों न हों, न तो एक नाप की हैं और न उनकी बनावट में कोई समानता है, न उनके पत्थर एक ढंग के हैं, न उनकी ऊँचाई-नीचाई एक-सी है, अर्थात हर सीढ़ी हर ढंग की है। जैसे हर इनसान की शक्ल जुदा-जुदा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ की सीढ़ियाँ जुदा-जुदा ढंग से बनाई गयी हैं। काशी की सीढ़ियों की यही सबसे बड़ी खूबी है।

अब आप मान लीजिए सीढ़ी के ऊपर हैं, नीचे तक गौर से सारी सीढ़ियाँ आपने देख लीं और एक नाप से कदम फेंकते हुए चल पड़े, पर तीसरी पर जहाँ अनुमान से आपका पैर पड़ना चाहिए नहीं पड़ा, बल्कि चौथी पर पड़ गया। आगे आप जरा सावधानी से साथ चलने लगे तो आठवीं सीढ़ी अन्दाज से कहीं अधिक नीची है, ऐसा अनुभव हुआ। अगर उस झटके से अपने को बचा सके तो गनीमत है, वरना कुछ दिनों के लिए अस्पताल में दाख़िल होना पड़ेगा। अब आप और भी सावधानी से आगे बढ़े तो बीसवीं सीढ़ी पर आपका पैर न गिरकर सतह पर ही पड़ जाता है और आपका अन्दाज़ा चूक जाता है। गौर से देखने पर आपने देखा यह सीढ़ी नहीं, चौड़ा फर्श है।
अब सवाल यह है कि आखिर बनारसवालों ने अपने मकान में, मन्दिर में, या अन्य जगह ऐसी खतरनाक सीढ़ियाँ क्यों बनवायीं? इसमें क्या तुक है? तो इसके लिए आपको जरा काशी का इतिहास उलटना पड़ेगा। बनारस जो पहले सारनाथ के पास था, खिसकते-खिसकते आज यहाँ आ गया है। यह कैसे खिसककर आ गया, यहाँ इस पर गौर करना नहीं है।
लेकिन बनारसवालों में एक खास आदत है, वह यह कि वे अधिक फैलाव में बसना नहीं चाहते, फिर गंगा, विश्वनाथ मन्दिर और बाजार के निकट रहना चाहते हैं। जब भी चाहा दन से गंगा में गोता मारा और ऊपर घर चले आये। बाजार से सामान खरीदा, विश्वनाथ-दर्शन किया, चट घर के भीतर।
फलस्वरूप गंगा के किनारे-किनारे घनी आबादी बसती गयी। जगह संकुचित, पर धूप खाने तथा गंगा की बहार लेने और पड़ोसियों की बराबरी में तीन-चार मंजिल मकान बनाना भी जरूरी है। अगर सारी जमीन सीढ़ियाँ ही खा जाएँगी तो मकान में रहने की जगह कहाँ रहेगी? फलस्वरूप ऊँची-नीची जैसे पत्थर की पटिया मिली, फिट कर दी गयी – लीजिए भैयाजी की हवेली तैयार हो गयी। चूँकि बनारसी सीढ़ियों पर चढ़ने-उतरने के आदी हो गये हैं, इसलिए उनके लिए ये खतरनाक नहीं हैं, पर मेहमानों तथा बाहरी अतिथियों के लिए यह अवश्य हैं।
सीढ़ियों का दृश्य काशी के घाटों में ही देखने को मिलता है। चूँकि काशी नगरी गंगा की सतह से काफी ऊँचे धरातल पर बसी है इसलिए यहाँ सीढ़ियों की बस्ती है। काशी के घाटों को आपने देखा होगा, उन पर टहले भी होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि केदारघाट पर कितनी सीढ़ियाँ हैं? सिन्धिया घाट पर कितनी सीढ़ियाँ हैं? शिवाले से त्रिलोचन तक कितनी बुर्जिंयाँ हैं? साफा लगाने लायक कौन-सा घाट अच्छा है? आप कहेंगे कि यह बेकार का सरदर्द कौन मोल ले। लेकिन जनाब, हरिभजन से लेकर बीड़ी बनानेवालों की आम सभाएँ इन्हीं घाटों पर होती हैं।
हज़ारों गुरु लोग इन घाटों पर साफा लगाते हैं, यहाँ कवि-सम्मेलन होते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, धर्मप्राण व्यक्ति सर्राटे से माला फेरते हैं, पंडे धोती की रखवाली करते हैं, तीर्थयात्री अपने चँदवे साफ करवाते हैं। यहाँ भिखमंगों की दुनिया आबाद रहती है और सबसे मजेदार बात यह है कि घर के उन निकलुओं को भी ये घाट अपने यहाँ शरण देते हैं जिनके दरवाजे आधी रात को नहीं खुलते। ये घाट की सीढ़ियाँ बनारस का विश्रामगृह हैं, जहाँ सोने पर पुलिस चालान नहीं करेगी, नगरपालिका टैक्स नहीं लेगी और न कोई आपको छेड़ेगा। ऐसी हैं बनारस की सीढ़ियाँ।